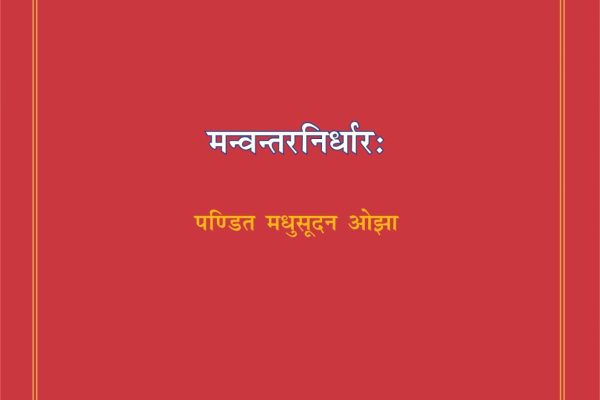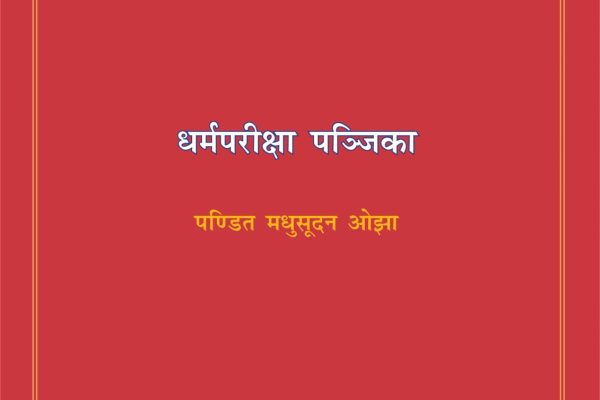प्रतिवेदनश्रीशंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ब्रह्मविज्ञानविमर्श शृंखला के अन्तर्गत दिनांक ३० मई २०२३ को शारीरकविमर्श विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का समायोजन अन्तर्जालीय माध्यम से किया गया। यह संगोष्ठी पण्डित मधुसूदन ओझा प्रणीत शारीरकविमर्श नामक ग्रन्थ के चार प्रकरणों को आधार बनाकर समायोजित थी। जिसमें पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी के संस्कृत विभाग के आचार्य. प्रो. के. ई. धरणीधरण ने मुख्य वक्ता के रूप में तथा अन्य वक्ताओं में प्रो. के. गणपति भट्ट, आचार्य, अद्वैतवेदान्त विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, डॉ. रामचन्द्र शर्मा, सह आचार्य, न्यायविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वद्यालय, नई दिल्ली तथा डॉ. देवेश कुमार मिश्र, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। यह संगोष्ठी श्रीशंकर शिक्षायतन के समन्वयक तथा संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रो. सन्तोष कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। पं. मधुसूदन ओझा प्रणीत शारीरकविर्मश अद्वैतवेदान्त का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक मौलिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में कुल सोलह प्रकरण हैं। जिसके पहले, दूसरे, तीसरे एवं पाँचवें प्रकरण को आधार बना कर वक्ताओं ने व्याख्यान दिये। ब्रह्म-मीमांसा-प्रवृत्तिनिमित्त नामक पहले प्रकरण के अनुसार ब्रह्म तत्त्व सृष्टि का मूल कारण है। मीमांसा का अर्थ विचार होता है। प्रवृत्तिनिमित्त का अर्थ कारण है। इस प्रकार ब्रह्म के विचार का जो कारण है। उस विषय पर विचार यहाँ प्रारंभ होता है। इस अध्याय में बारह उपशीर्षक हैं। जिसमें पं. ओझा जी ने सृष्टि के मूलकारण के रूप में क्रमशः दैवतत्त्व, रजस्तत्त्व, अपरतत्त्व, आपतत्त्व, वाक्-तत्त्व, व्योमतत्त्व, सदसत्-तत्त्व, अमृतमृत्युतत्त्व एवं संशयतत्त्व को उपस्थापित किया है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रो. के. ई. धरणीधरण ने इसी प्रकरण पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में सृष्टिकारक प्रत्येक तत्त्व पर विचार करते हुए कहा कि सृष्टि वाक् तत्त्व से होती है, यह व्याकरणदर्शन का सिद्धान्त है। श्रुति में ‘वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे’ यह वाक्य प्राप्त होता है। विश्व की सृष्टि में ब्रह्म मूल कारण है। वह ब्रह्म तत्त्व एक है अथवा अनेक। इस पर विचार करते हुए ग्रन्थकार पं. ओझा जी ने कहा कि सृष्टि से पूर्व ब्रह्म तत्त्व ही था । (‘ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् एकमेव’, बृहदारण्यक उपनिषद् १.४.१०) ब्रह्म तत्त्व एक ही है, अनेक नहीं है। ‘तथा चेदं ब्रह्मैकमेवेति सिद्धान्तः।’ (शारीरकविमर्श, पृ.१०, हिन्दी अनुवाद संस्करण) दूसरे प्रकरण का नाम शास्त्र-ब्रह्म-मीमांसा है। यहाँ शास्त्र का अर्थ श्रुति है। ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रिय ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं है। अनुमान से ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पर ही होता है। उपमान से ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म के समान कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। शब्द से भी ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता है क्योंकि शब्द में भी ब्रह्म को बतलाने की शक्ति नहीं है। फिर भी शब्द ब्रह्म का संकेत मात्र करता है । वैदिकविज्ञान में शास्त्र का अर्थ वेद है और वह वेद ही ब्रह्म है। उस पर विचार करना यह शास्त्र-ब्रह्म-मीमांसा का अर्थ होता है। इस प्रकरण में छः उपशीर्षक हैं।इसी प्रकरण को आधार बना कर प्रो. के. गणपति भट्ट, ने अपने व्याख्यान में कहा कि ग्रन्थकार पं. ओझा जी ने ब्रह्म के दो स्वरूपों का प्रतिपादन किया है। एक आत्मब्रह्म है और दूसरा शास्त्रब्रह्म है। ग्रन्थकार पं. ओझा जी ने बृहदारण्यक उपनिषद् के आधार पर आत्मा को वाङ्मय, प्राणमय और मनोमय इन तीन रूपों में व्याख्यायित किया है तथा इसी के आधार पर आत्मा के तीन भावों को विविध रूपों में उद्धाटित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। आत्मा के तीन भाव हैं- शान्तभाव, वीरभाव और पशुभाव । आत्मा के तीन तन्त्र हैं। यहाँ तन्त्र का अर्थ स्वरूप से है। आत्मा के तीन स्वरूप हैं- ज्ञान, कर्म और अर्थ। इन तीन तन्त्रों के द्योतक तीन वीर्य हैं। वीर्य का अर्थ सामर्थ्य होता है। आत्मा के तीन वीर्य हैं- ब्रह्म, क्षत्र और विट्। ब्रह्मवीर्य का अर्थ करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि ज्ञान के उदय का जो साधन प्रतिभा अथवा तेज है वही ब्रह्म वीर्य है- ‘तत्र ज्ञानोदयौपयिकं वर्चोलक्षणं ब्रह्मवीर्यम्।’( शारीरकविमर्श, पृ. २७) कर्म की प्राप्ति उत्साह से होती है, यही क्षत्रवीर्य है। धन की प्राप्ति संग्रह से होती है, यह वीड्वीर्य है-“कर्मोदयौपयिकमित्साहलक्षणं क्षत्रवीर्यम्,वित्तसंचयौपयिकं संग्रहलक्षणं विड्वीर्यम्।” (वही) तीसरे प्रकरण का नाम वेदतत्त्वनिरुक्ति है। जिस प्रकार अद्वैतवेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि होती है, न्याय-वैशेषिक में परमाणु से सृष्टि होती है, सांख्य-योग में प्रकृति और पुरुष से सृष्टि होती है। उसी प्रकार वैदिकविज्ञान में वेदतत्त्व से सृष्टि होती है। इस प्रकरण में कुल ग्यारह उपशीर्षक हैं। इसी प्रकरण को आधार बना कर डॉ. रामचन्द्र शर्मा, सह आचार्य, न्यायविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वद्यालय, नई दिल्ली ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया । उन्होंने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रन्थकार ने वेदतत्त्व को अनेक रूपों में व्याख्यायित किया है। वाक् तत्त्व से सृष्टि होती है। वाक् तत्त्व मन और प्राण से हमेशा युक्त रहता है। सत्य स्वरूप वाली वाक् से ये (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद) वेद हैं। ये वेद आत्मा की ही महिमा हैं। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है। (सर्वं खल्विदं ब्रह्म)। प्रजापति ने इस विश्व को तीन रूपों में विभक्त किया है- ज्ञान, क्रिया और अर्थ। (१) ज्ञान के तीन रूप हैं- आनन्द, विज्ञान और मन। इस ज्ञान का जो प्रधान पुरुष है, वही चिदात्मा कहलाता है। इस चिदात्मा का जो महिमा है, वह मनोमय वेद है। (२) कर्म भी तीन प्रकार के हैं- मन, प्राण और वाक्। कर्म के प्रधान पुरुष को कर्मात्मा कहा जाता है। कर्मात्मा की महिमा प्राणमय वेद है। (३) अर्थ तीन प्रकार के हैं- वाक्, अप् और अग्नि। इस का जो प्रधान पुरुष है, वह भूतात्मा कहलाता है। इस भूतात्मा की महिमा वाङ्मय वेद है। ‘त्रयी वा एष विद्या तपति’ इस श्रुति वाक्य की अभिनव व्याख्या यहाँ प्राप्त होता है। पाँचवें प्रकरण का नाम वेदशाखाविभाग है। वेद की कितनी शाखायें हैं। इस विषय पर यहाँ चर्चा की गयी है। विज्ञानवेद और शास्त्रवेद इन दोनों वेद के समान रूप से विभाग होने पर वेद के एक हजार एक सौ इकतीस शाखाएँ हैं। इस प्रकरण के आधार पर व्याख्यान करते हुए डॉ. देवेश कुमार मिश्र ने बतलया कि वैदिकविज्ञान में ऋत और सत्य ये दो सृष्टिप्रतिपादक सैद्धान्तिक तत्त्व हैं। ऋत का अर्थ शून्य और सत्य का अर्थ पूर्ण होता है। आप (जल) तत्त्व ऋत और…